क्रिया |
|
| क्रिया जिन शब्दों के माध्यम से कार्य को करने या होने का बोध होता है, वे क्रिया कहलाते हैं । क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं । हिंदी भाषा में क्रिया वाक्य के मध्य या अन्त कहीं भी हो सकती है । क्रिया विकारी शब्द है, इस पर लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि का प्रभाव पड़ता है । यदि कर्ता के साथ विभक्ति चिह्न न लगा हो,तो क्रिया का लिंग, वचन कर्ता के अनुसार होता है । यदि कर्ता के साथ विभक्ति चिह्न लगा हो,तो क्रिया कर्म के अनुसार आती है । यदि वाक्य के कर्ता और कर्म दोनों के साथ विभक्ति चिह्नो का प्रयोग हो,तो वाक्य की क्रिया सदैव एकवचन पुल्लिंग होती है क्रिया का सामान्य रूप धातु में ‘ना’ जुड़ने से बनता है । |
|
क्रिया के भेद
|
|
| क्रिया के भेद क्रिया के भेद हम दो आधारों पर कर सकते हैं- (क) कर्म के आधार पर भेद (ख) संरचना अथवा प्रयोग के आधार पर भेद (क) कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कर्म के आधार पर क्रिया के भेद निम्न दो प्रकार हैं- अकर्मक क्रिया -जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म नही होता है ,वह अकर्मक क्रिया कहलाती है । जैसे- मोहन लिखता है । यहाँ लिखना अकर्मक क्रिया है । सकर्मक क्रिया – जब वाक्य में क्रिया के साथ-साथ कर्म भी हो, तो वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है । जैसे- राधा गाना गाती है । यहाँ गाना सकर्मक क्रिया है । सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती है- (अ) एक कर्मक क्रिया- जिस वाक्य में एक कर्म होता है । (ब) द्विकर्मक क्रिया – जिस वाक्य में दो कर्म होते हैं । (ख) संरचना के आधार पर क्रिया के भेद |
|
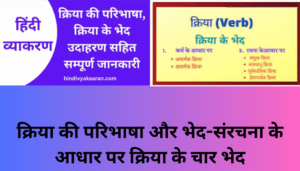
संरचना के आधार पर क्रिया के चार भेद |
| संरचना के आधार पर क्रिया के चार भेद संयुक्त क्रिया नामधातु क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया पूर्वकालिक क्रिया संयुक्त क्रिया जब दो या दो अधिक क्रियाओं से मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं । जैसे- तुम मेरे घर आ जाया करो । नामधातु क्रिया क्रिया को छोड़कर अन्य शब्दों(संज्ञा,सर्वनाम और विशेषण) में प्रत्यय जोड़ने से जो धातुएँ बनती हैं, उन्हें नामधातु क्रिया कहते हैं । जैसे- बात- बताना , हाथ- हथियाना ,अपना- अपनाना, गरम- गरमाना आदि । प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और को कार्य के लिए प्रेरित करता है, तो क्रिया प्रेरणार्थक कहलाती है । राजेश सोहन से कपडे धुलवाता है । पूर्वकालिक क्रिया वह क्रिया जो मुख्य क्रिया से पहले आती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है । |
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अनुकरणवाची शब्दों से निर्मित कुछ नामधातु क्रियाएँ
|
| संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अनुकरणवाची शब्दों से निर्मित कुछ नामधातु क्रियाएँ संज्ञा शब्द – नामधातु क्रिया शर्म – शर्माना लोभ – लुभाना बात – बतियाना झूठ – झुठलाना लात – लतियाना दुख – दुखाना सर्वनाम शब्द – नामधातु क्रिया अपना – अपनाना विशेषण शब्द – नामधातु क्रिया साठ – सठियाना तोतला – तुतलाना नरम – नरमाना गरम – गरमाना लज्जा – लजाना लालच – ललचाना फ़िल्म – फिल्माना अनुकरणवाची शब्द – नामधातु क्रिया थप-थप – थपथपाना थर-थर – थरथराना कँप-कँप – कँपकँपाना टन-टन – टनटनाना बड़-बड़ – बड़बड़ाना खट-खट – खटखटाना घर-घर – घरघराना द्रष्टव्य- नामबोधक क्रियाएँ संयुक्त क्रियाएँ नहीं हैं। संयुक्त क्रियाएँ दो क्रियाओं के योग से बनती है और नामबोधक क्रियाएँ संज्ञा अथवा विशेषण के मेल से बनती है। दोनों में यही अन्तर है। |
प्रेरणार्थक क्रिया (Causative Verb)
|
| प्रेरणार्थक क्रिया (Causative Verb) जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे तो उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे- काटना से कटवाना, करना से कराना। एक अन्य उदाहरण इस प्रकार है- मालिक नौकर से कार साफ करवाता है। अध्यापिका छात्र से पाठ पढ़वाती हैं। उपर्युक्त वाक्यों में मालिक तथा अध्यापिका प्रेरणा देने वाले कर्ता हैं। नौकर तथा छात्र को प्रेरित किया जा रहा है। अतः उपर्युक्त वाक्यों में करवाता तथा पढ़वाती प्रेरणार्थक क्रियाएँ हैं। प्रेरणार्थक क्रिया में दो कर्ता होते हैं : (1) प्रेरक कर्ता-प्रेरणा देने वाला; जैसे- मालिक, अध्यापिका आदि। (2) प्रेरित कर्ता-प्रेरित होने वाला अर्थात जिसे प्रेरणा दी जा रही है; जैसे- नौकर, छात्र आदि। |
प्रेरणार्थक क्रिया के रूप
|
| प्रेरणार्थक क्रिया के रूप प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप हैं : (1) प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया (2) द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया (1) प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया माँ परिवार के लिए भोजन बनाती है। जोकर सर्कस में खेल दिखाता है। रानी अनिमेष को खाना खिलाती है। नौकरानी बच्चे को झूला झुलाती है। इन वाक्यों में कर्ता प्रेरक बनकर प्रेरणा दे रहा है। अतः ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण हैं। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएँ सकर्मक होती हैं। (2) द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया माँ पुत्री से भोजन बनवाती है। जोकर सर्कस में हाथी से करतब करवाता है। रानी राधा से अनिमेष को खाना खिलवाती है। माँ नौकरानी से बच्चे को झूला झुलवाती है। इन वाक्यों में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है और दूसरे से कार्य करवा रहा है। अतः यहाँ द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक-दोनों में क्रियाएँ एक ही हो रही हैं, परन्तु उनको करने और करवाने वाले कर्ता अलग-अलग हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया प्रत्यक्ष होती है तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया अप्रत्यक्ष होती है। याद रखने वाली बात यह है कि अकर्मक क्रिया प्रेरणार्थक होने पर सकर्मक (कर्म लेनेवाली) हो जाती है। जैसे- राम लजाता है। वह राम को लजवाता है। प्रेरणार्थक क्रियाएँ सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं। ऐसी क्रियाएँ हर स्थिति में सकर्मक ही रहती हैं। जैसे- मैंने उसे हँसाया; मैंने उससे किताब लिखवायी। पहले में कर्ता अन्य (कर्म) को हँसाता है और दूसरे में कर्ता दूसरे को किताब लिखने को प्रेरित करता है। इस प्रकार हिन्दी में प्रेरणार्थक क्रियाओं के दो रूप चलते हैं। प्रथम में ‘ना’ का और द्वितीय में ‘वाना’ का प्रयोग होता है- हँसाना- हँसवाना। |
निष्कर्ष:
संरचना के आधार पर क्रिया के ये चार भेद भाषा में क्रिया की भूमिका को स्पष्ट करने में सहायक होते हैं। ये भेद यह बताते हैं कि क्रिया वाक्य में मुख्य कार्य कर रही है या केवल सहायता प्रदान कर रही है, और यह भी कि वह कर्म पर कार्य कर रही है या नहीं। क्रिया की सही पहचान वाक्य की संरचना को समझने के लिए आवश्यक है
